झारखंड—एक राज्य जो अपनी विशाल प्राकृतिक संपदाओं और जीवंत आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है—इन दिनों एक गंभीर कानूनी और नैतिक टकराव से गुजर रहा है। यह टकराव आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की संवैधानिक कोशिशों और औद्योगिक विकास की तीव्र मांगों के बीच है। इस संघर्ष के केंद्र में है पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)—एक ऐसा कानून, जिसे आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि, संसाधनों और संस्कृति पर स्वशासन का अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन व्यवहार में यह कानून अक्सर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियों से टकराता रहा है, जिससे आदिवासी स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है।
पेसा अधिनियम का मूल उद्देश्य यह था कि आदिवासी समुदायों को अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास या संसाधन दोहन से जुड़े फैसलों में सीधी भागीदारी मिले। ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी परियोजना को मंजूरी दें या अस्वीकार करें। लेकिन यह आदर्श स्थिति अब तक ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाई है। वरिष्ठ राजनेता सरयू राय कहते हैं, “पेसा एक क्रांतिकारी कानून होना चाहिए था, लेकिन यह कागज़ों में ही सिमट कर रह गया है।”
उनका मानना है कि झारखंड की सरकारें लगातार पेसा के सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ करती रही हैं। “स्थानीय समुदायों की वास्तविक चिंताओं को अक्सर किनारे कर दिया जाता है। झारखंड में अब तक की सभी सरकारों ने स्थानीय स्वशासन के इस संवैधानिक प्रावधान की उपेक्षा की है,” वे जोड़ते हैं।
इस समस्या की जड़ है—पेसा और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य कानूनों के बीच का टकराव। भूमि अधिग्रहण अधिनियम और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम (MMDR Act) जैसे कानून औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना के नाम पर भूमि और संसाधनों के अधिग्रहण को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर पेसा की उस ज़रूरी शर्त को दरकिनार कर देती है, जिसमें ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। नतीजतन, विकास की योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भूमिका खत्म होती जा रही है, और उनकी स्वायत्तता लगातार कमजोर हो रही है।
इस टकराव को न्यायपालिका ने भी नजरअंदाज़ नहीं किया है। 29 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह दो महीने के भीतर पेसा नियमों को लागू करे। यह आदेश आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था। लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं।
आदिवासी कार्यकर्ताओं के लिए यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि न्याय और शासन का है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता संजय मेहता कहते हैं, “झारखंड में विकास बनाम आदिवासी अधिकार का टकराव केवल विधिक मुद्दा नहीं है, यह शासन और सामाजिक न्याय का मूल प्रश्न है।”
प्रमुख राजनीतिक नेता और आदिवासी आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा का मानना है कि पेसा लागू न होने के पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। वे कहते हैं, “अगर राज्य सरकार की मंशा सही होती, तो पेसा कब का लागू हो चुका होता। चाहे जेएमएम हो या बीजेपी—सभी दलों ने इस संवैधानिक अधिकार के खिलाफ काम किया है।”
इस मुद्दे को लेकर आदिवासी समुदाय सक्रिय हो गया है। 32 आदिवासी एवं मूलवासी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिलने वाला है। उनकी मांग है कि राज्य में पेसा को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। बेसरा छत्तीसगढ़ के पेसा नियम 2022 को एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं और झारखंड से ऐसी ही नीति लागू करने की अपील करते हैं।
पेसा बनाम राज्य और राष्ट्रीय कानूनों की यह लड़ाई झारखंड के आदिवासी भविष्य की दिशा तय करेगी। मुख्य प्रश्न यह है—क्या राज्य आर्थिक विकास को आदिवासी स्वायत्तता से ऊपर रखेगा, या क्या वह संविधान में निहित स्वशासन के वादे को निभाएगा? इस संघर्ष का हल आदिवासी समाज की नियति को परिभाषित करेगा और यह भी तय करेगा कि झारखंड अपने मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा में कितना गंभीर है।
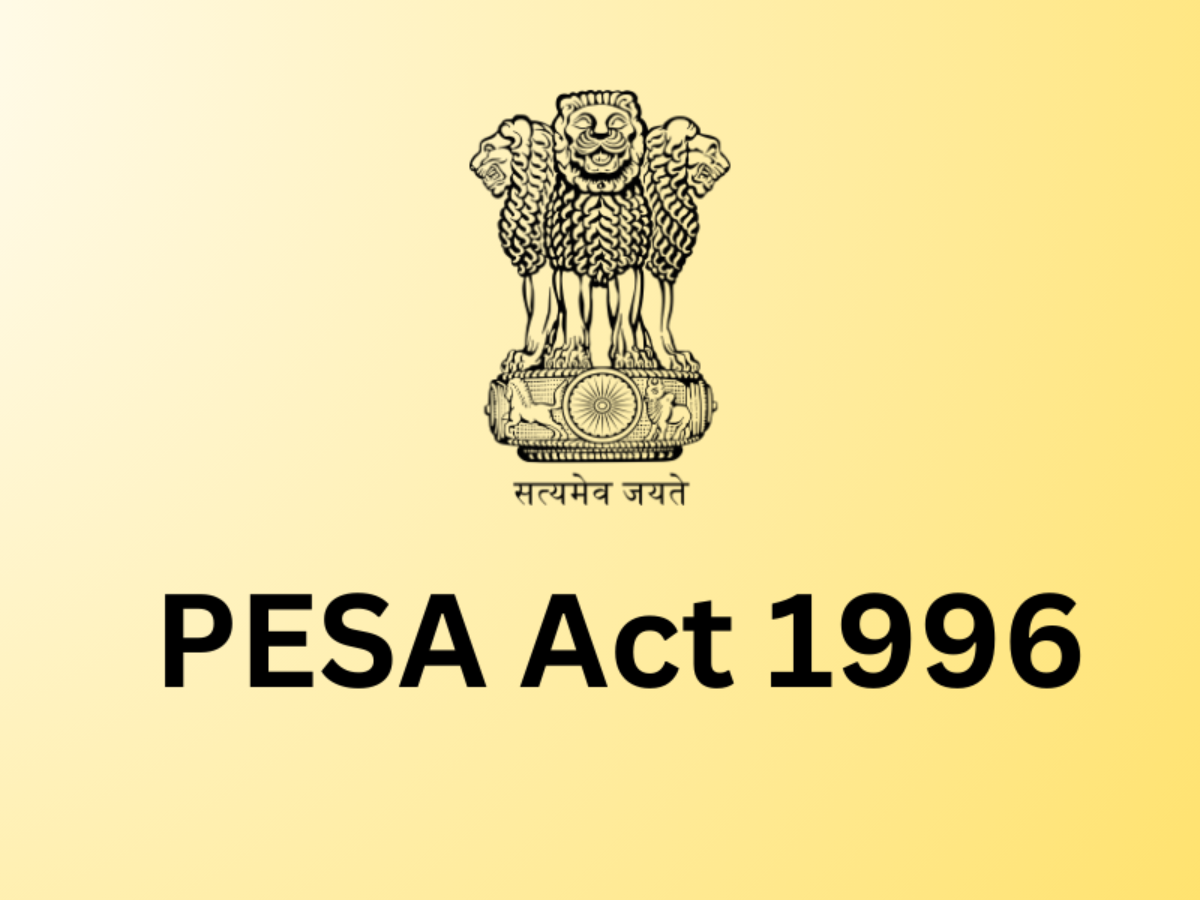

 वीडियो2 months ago
वीडियो2 months ago
 वीडियो3 weeks ago
वीडियो3 weeks ago
 राँची सभा3 weeks ago
राँची सभा3 weeks ago
 राँची सभा3 weeks ago
राँची सभा3 weeks ago
 राँची सभा3 weeks ago
राँची सभा3 weeks ago
 हजारीबाग सभा3 weeks ago
हजारीबाग सभा3 weeks ago
 राँची सभा3 weeks ago
राँची सभा3 weeks ago
 वीडियो3 weeks ago
वीडियो3 weeks ago






